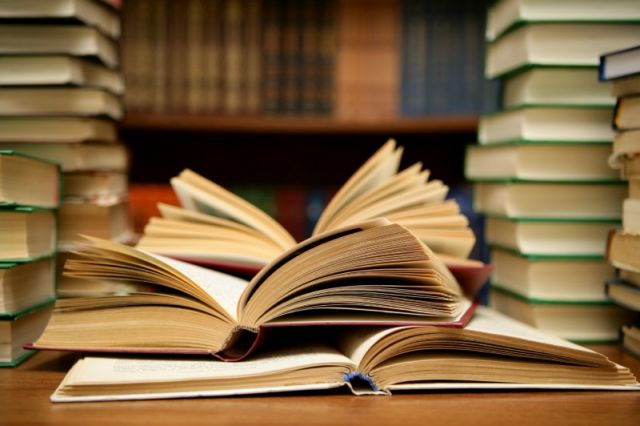हिंदी के विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम जाति-विद्वेष, सांस्कृतिक विद्वेष और धर्म-विद्वेष को बढ़ावा देनेवाले पाठ्यक्रम हैं। इन पाठ्यक्रमों में हमारे सांस्कृतिक नायकों और मूल्यों के प्रति द्वेष को बढ़ावा दिया गया है। घृणा के कृत्रिम केन्द्र तैयार किये गए हैं। तथाकथित सवर्णों, विषयों और मिथकीय प्रतीकों को घृणा का केंद्र बनाकर पाठ्य-पुस्तकें लगाई गई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी के विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों को ‘डी टॉक्सिपफाई’ करना पड़ेगा। पाठ्यक्रमों के माध्यम से वामपंथी वैचारिक दुराग्रहों और राजनीतिक निहितार्थों को पूरा करने का जो कुचक्र चल रहा है – उसे समझना होगा।
सन् 1990 ई. में हिंदी में औपचारिक नामांकन हुआ. बी.ए, एम.ए, एम.फिल, पीएच. डी. फिर अध्यापन। समय बदला, देश का मिजाज बदला, पर हिंदी के विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम का स्वर नहीं बदला। वही प्रलेस, जलेस-मार्का कार्यकर्ता-अध्यापक लोग, वही पात्रों के वर्ग-चरित्र की व्याख्याएँ, वही द्वन्द्व खोजने की वृत्ति बनी रही। बदलने के नाम पर यौनिकता, लैंगिकता, स्त्री-देह और जातिवाद पर शोध करने को बढ़ावा देने की वृत्ति बढ़ी। ऐसा लगा जैसे हिंदी-समाज की बाकी समस्याएँ खत्म हो गईं और सेक्स ही सबसे बड़ी समस्या है।
हिंदी के क्रांतिकारी, कार्यकर्ता-आचार्यों को देख लीजिए, उनके शोध-विषय स्त्री-देह, स्त्री-समलैंगिकता, पुरुष-समलैंगिकता जैसे विषयों पर ही केंद्रित हैं। मेरी मान्यता है कि हिंदी के विभाग सेक्सुअली पोवर्टेड और सेक्स ऑब्सेस्ड विभाग हैं। इसकी छाया हिंदी के पाठ्यक्रमों में देखी जा सकती है।
मेरा आरोप है कि देश के विश्वविद्यालयों का हिंदी पाठ्यक्रम एक निम्नस्तरीय राजनीतिक चेतना (थर्ड रेट पॉलिटिकल कान्ससनेस) का विभाग है। सिवान, बलिया, बनारस, गोपालगंज, जीयनपुर और गोपालन भवन से आए हुए लुगदी मार्का आचार्यों द्वारा पचास-साठ के दशक से उधार लिए गए शब्दों से बना, किसी द्विवेदी जी या किसी सेठ के यहाँ चटनी बनाते हुए सीखे गए वर्ग-विरोध, वर्ग-संघर्ष, बुर्जुआ, सर्वहारा, क्रांति की शब्दावली से बना हुआ यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सामाजिक वास्तविकता से दूर करने वाला है। हिंदी क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों में यह पाठ्यक्रम अनावश्यक आक्रामकता पैदा करता है।
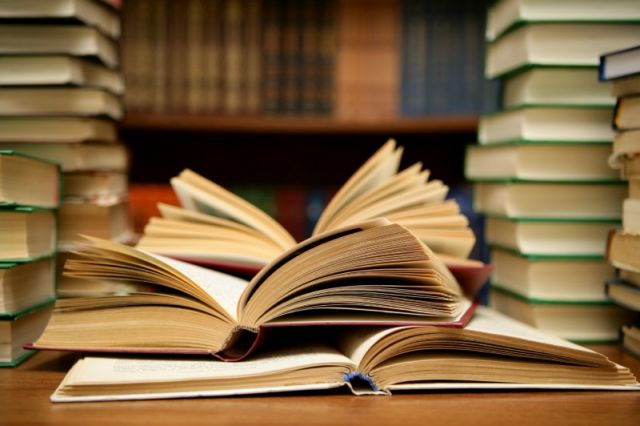
हिंदी की विश्वविद्यालयी शिक्षा अपनी शरण में आये विद्यार्थियों को समाज, पूँजी और व्यवस्था के प्रति अनावश्यक रूप से आक्रामक बनाती है। हमारा विद्यार्थी जो पढ़कर जाता है, वह व्यवस्था के किसी काम का नहीं; चाहे वह पत्राकारिता की पढ़ाई हो या अनुवाद की। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विश्वविद्यालय से निकलने के बाद उसे एक अनलर्निंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि हिंदी का विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम समाज और सच्चाई से कटा हुआ पाठ्यक्रम है।
समाज और हिंदी विभागों की लड़ाई में समाज जीत गया, विभाग हार गये। समाज के कवि हिंदी के पाठ्यक्रमों के कवि नहीं हैं और हिंदी पाठ्यक्रमों के कवि समाज के कवि नहीं हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि विश्वविद्यालयों के हिंदी-विभागों में ‘महान’ बनाने का एक ‘बौद्धिक उद्योग’ चलता है। गोपालगंज, बनारस, सिवान, बलिया और खुर्जा से आया हुआ विद्यार्थी बीस हजार की नौकरी मांगता है, तो पाठ्यक्रम सिखाते हैं कि कवि बन जाओ, जलेस-प्रलेस मार्का आलोचक बन जाओ या फिर किसी आचार्य जी के यहाँ गमले में पानी डालो और फेसबुक पर ‘वाह-वाह’ करो।
विभागों का काम कवि बनाना और कहानीकार बनाना नहीं है। जिसे कवि और कहानीकार बनना होगा, वो किसी आचार्य जी के गमले के भरोसे नहीं बैठेगा। विश्वविद्यालयों का काम विद्यार्थी को ‘इम्पावर’ करना है; उसे तैयार करना है कि वह समाज की चुनौतियों का मुकाबला कर सके और अपने लिए दो जून की रोटी तलाश सके।
हिंदी के विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों को विद्यार्थियों के हिसाब से बदलना होगा। मैं अक्सर कहता हूँ आचार्य जी लोगों से कि इस यौनिकता और चेतना मार्का विमर्श से बाहर निकलिए और सत्रह साल के बच्चे की आँख से दुनिया देखिए जो अभी-अभी महाविद्यालय में हिंदी पढ़ने आया है। दो लाख रुपये वेतन लेकर समाज के मुख्यधारा में पीछे छूट गए विद्यार्थी को ‘आह’ और ‘वाह’ सिखाना, देश के करदाता का पैसा ‘रामदास’ और ‘चाँद का मुंह टेढ़ा है’ जैसी चीजों पर बर्बाद करना एक बौद्धिक घोटाला है। पचास वर्ष के हिंदी का विश्वविद्यालयी-पाठ्यक्रम अनवरत चल रहे इस बौद्धिक घोटाले का साक्ष्य है। हिंदी को बचाना है, तो उसे उस पूँजी और तकनीक के इलाके में प्रवेश करना होगा।

हिंदी के विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम जाति-विद्वेष, सांस्कृतिक विद्वेष और धर्म-विद्वेष को बढ़ावा देनेवाले पाठ्यक्रम हैं। इन पाठ्यक्रमों में हमारे सांस्कृतिक नायकों और मूल्यों के प्रति द्वेष को बढ़ावा दिया गया है। घृणा के कृत्रिम केन्द्र तैयार किये गए हैं। तथाकथित सवर्णों, विषयों और मिथकीय प्रतीकों को घृणा का केंद्र बनाकर पाठ्य-पुस्तकें लगाई गई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी के विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों को ‘डी टॉक्सिपफाई’ करना पड़ेगा।
पाठ्यक्रमों के माध्यम से वामपंथी वैचारिक दुराग्रहों और राजनीतिक निहितार्थों को पूरा करने का जो कुचक्र चल रहा है – उसे समझना होगा। हिंदी साहित्य का भविष्य हो ना हो, हिंदी भाषा का भविष्य अवश्य है। हिंदी विभागों को अगर बचाना है, तो उन्हें हिंदी भाषा, हिंदी पत्रकारिता, हिंदी अनुवाद और हिंदी रंगमंच के विभागों में बदलना होगा। सिर्फ ‘कच्ची सड़क के गाँव के ओर जाने’ और ‘बैगन के खेत में शौच करने’ के ठाकुर साहेब मार्का किस्सों से ना तो हिंदी का भला होगा, ना हिंदी पढ़ानेवालों का।
(लेखक हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)